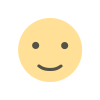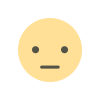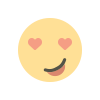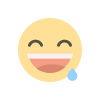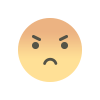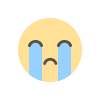जज वर्मा मामले से जजों की नियुक्ति में केंद्र को मिला मौका
दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर मिले लाखों रुपए के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादलों में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया है। केंद्र सरकार ने संसद में कॉलेजियम व्यवस्था के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का कानून पारित किया था। इस कानून के एक विवादास्पद प्रावधानों में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में भारत के प्रधान न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम जजों और केन्द्रीय कानून मंत्री के अलावा दो जानी मानी हस्तियों को शामिल करने की व्यवस्था थी। वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून-एनजेएसी को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था। जस्टिस वर्मा नोट प्रकरण के बाद न्यायिक नियुक्ति आयोग फिर से लागू करने की संभावना के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की उम्मीद फिर से पैदा हो गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में राजनीतिक दलों से कहा कि उन्हें जजों की तरफ से जजों की नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक तंत्र के बारे में सोचना चाहिए। धनखड़ ने कानून को रद्द करने के शीर्ष अदालत के फैसले को गलत बताया। उन्होंने वर्ष 2014 में सर्वसम्मति से बनाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को दूरदर्शी कदम बताया। इसका उद्देश्य एससी और एचसी के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के एकाधिकार को समाप्त करना था। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खडग़े और टीएमसी के सुखेंदु शेखर रॉय सहित विपक्षी नेताओं ने सरकार से उन कदमों की रूपरेखा तैयार करने को कहा है जो वह उठाना चाहती है। इसे भी पढ़ें: जज अपनी संपत्ति सार्वजनिक क्यों नहीं करते? क्या इसको लेकर नहीं है कोई आचार संहिता या कानूनजज कैशकांड के बाद सुप्रीम कोर्ट की फजीहत दो कारणों से हो रही है। न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द करने और जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने से। आयोग को रद्द करने पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति धनखड़ द्वारा राजनीतिक दलों की बैठक के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक आयोग को निरस्त करने के फैसले की तीखी भर्त्सना की गई। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाइकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले का विरोध किया है। एसोसिएशन ने हड़ताल के अलावा जस्टिस वर्मा की कोर्ट के बहिष्कार की चेतावनी दी है। जस्टिस वर्मा प्रकरण के बाद सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम द्वारा हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर फिर से उंगलियां उठने लगी हैं। न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं होने और इनमें परिवारवाद को वरीयता दिए जाने को "अंकल जज सिंड्रोम" कहते हैं। जब जज बनाने के लिए अधिवक्ताओं के नाम प्रस्तावित किए जाते हैं तो किसी भी स्तर पर किसी से कोई राय नहीं ली जाती। ऐसे में जिन लोगों का नाम प्रस्तावित किया जाता है, उनमें से कई पूर्व न्यायाधीशों के परिवार से होते हैं या उनके संबंधी होते हैं। भारतीय विधि आयोग ने अपनी 230वीं रिपोर्ट में उच्च न्यायालयों में 'अंकल जजों' की नियुक्ति के मामले का उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है कि जिन जजों के परिजन किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं, उन्हें उसी उच्च न्यायालय में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। विवादों में घिरे जस्टिस वर्मा का अकेला मामला नहीं है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष परेशानी खड़ी हुई है। पूर्व में हाईकोर्ट के जजों खिलाफ इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूरी जानकारी मांगी वहीं, संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग ने जोर पकड़ा। जस्टिस वी. रामास्वामी पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू की गई थी। उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव 1993 में लोकसभा में लाया गया था। लेकिन यह प्रस्ताव गिर गया था क्योंकि उसे जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं हो सका। जस्टिस रामास्वामी 1990 में पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश थे तब उन पर आधिकारिक तौर पर अलॉट किए गए घर पर कब्जा किए जाने का आरोप लगा था। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन देश के दूसरे जज थे जिन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा था। उनके खिलाफ 2011 में राज्य सभा द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। जस्टिस सौमित्र सेन ने महाभियोग चलाए जाने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल को अपना इस्तीफा भेज दिया था। वह पहले ऐसे न्यायाधीश थे जिन पर उच्च सदन द्वारा कदाचार के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। वर्ष 2015 में राज्यसभा के 58 सदस्यों ने गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस जे.बी. पारदीवाला के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था। जेबी पारदीवाला ने आरक्षण के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सांसदों ने अपने प्रस्ताव में अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ उनके अपशब्द कहे जाने पर आपत्ति जताई थी। उस समय उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी के पास महाभियोग का प्रस्ताव भेजे जाने के बाद जस्टिस पारदीवाला ने अपने फैसले से वह शब्द हटा लिए थे। भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोपों पर सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी.डी. दिनाकरन के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी की गई थी। लेकिन सुनवाई के कुछ दिनों पहले ही दिनाकरन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दिनाकरन पर जमीन पर कब्जा करने और आय से अधिक संपत्ति के मामले थे। इसके अलावा 2017 में राज्यसभा सांसदों ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस सी.वी. नागार्जुन रेड्डी के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया था। मार्च 2018 में विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र

जज वर्मा मामले से जजों की नियुक्ति में केंद्र को मिला मौका
नेता नगरी - जज वर्मा मामले ने भारतीय न्यायपालिका की नियुक्ति प्रक्रिया में एक नए मोड़ को जन्म दिया है। यह मामला न केवल जजों की नियुक्तियों के लिए केंद्र सरकार को बड़ा अवसर प्रदान कर रहा है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे इस मामले की पृष्ठभूमि, निहितार्थ और आगे की संभावनाओं के बारे में।
जज वर्मा मामला: पृष्ठभूमि
जज वर्मा की नियुक्ति के विवाद ने देश की न्यायपालिका में चर्चाएँ बढ़ा दी हैं। जज वर्मा को उनकी योग्यता और कार्यशैली के लिए जाना जाता है, लेकिन उनकी नियुक्ति को लेकर कुछ राजनीतिक विवाद उठ खड़े हुए हैं। इस संदर्भ में, जिस समय जज वर्मा के मामले की चर्चा हुई, तब केन्द्र सरकार ने उनके मामले को आधार बनाकर जजों की नियुक्तियों में कुछ अपेक्षित बदलावों को लागू करने का सोचना शुरू किया।
केंद्र सरकार का नया दृष्टिकोण
केंद्र सरकार ने जजों की नियुक्तियों में प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है, ताकि न्यायपालिका की पारदर्शिता और कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सके। इससे न केवल जज वर्मा जैसे विवादित मामलों से निपटने में मदद मिलेगी, बल्कि न्यायपालिका में निष्पक्षता भी सुनिश्चित होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बहाल होगा।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ
जज वर्मा मामले पर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच तीखी प्रतिक्रियाएँ आई हैं। कुछ नेताओं ने सरकार की नीतियों की प्रशंसा की है, जबकि अन्य ने इस प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप होने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाए हैं। यह विवाद विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है, जहाँ एक ओर न्यायपालिका की स्वायत्तता और दूसरी ओर राजनीति के खेल का महत्व है।
भविष्य की संभावनाएँ
जज वर्मा मामले ने नई नियुक्तियों की प्रक्रिया में एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है। यदि सरकार सही दिशा में काम करती है, तो यह न्यायपालिका में सुधार का एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इसके साथ ही, नागरिकों का न्यायिक प्रणाली पर विश्वास बढ़ाने में भी सहायता मिल सकती है।
निष्कर्ष
जज वर्मा मामले की घटनाएँ न केवल वर्तमान में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि दीर्घकालिक प्रभाव भी डाल सकती हैं। केंद्र सरकार के लिए यह एक अवसर है कि वह न्यायपालिका में सुधार लाए और इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाए। हमें उम्मीद है कि यह मामला देश की न्याय प्रणाली में सकारात्मक बदलाव लाएगा।
लेखन टीम: नीता शर्मा, स्वाति अग्रवाल, टीम नेता नगरी
Keywords
judge Verma case, judicial appointments, central government, judiciary reforms, political reactions, transparency in judiciaryWhat's Your Reaction?